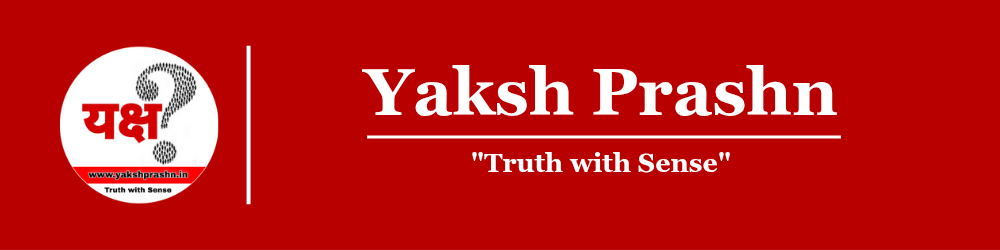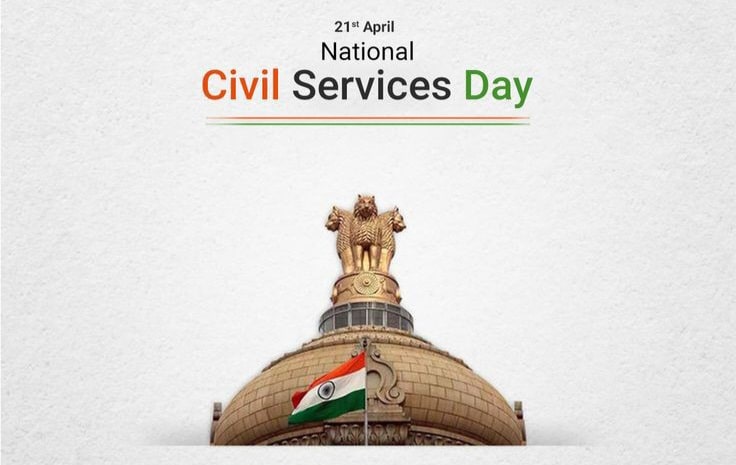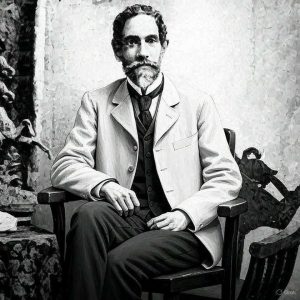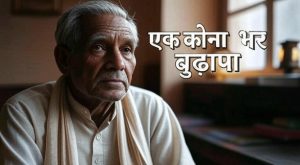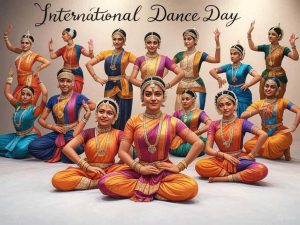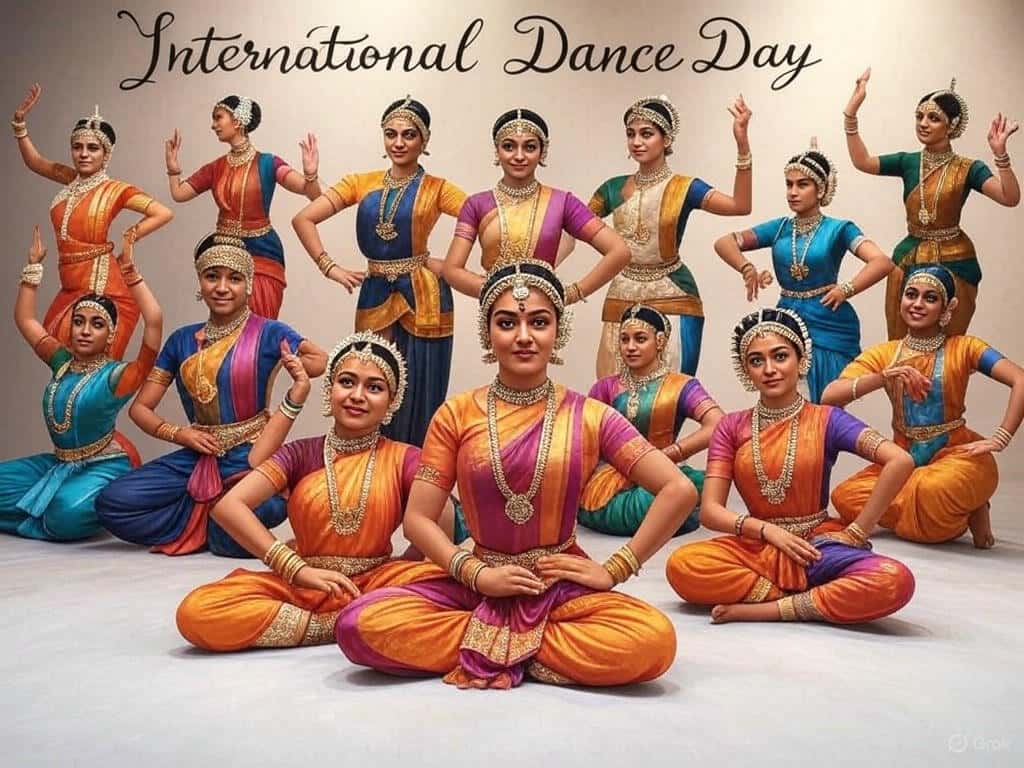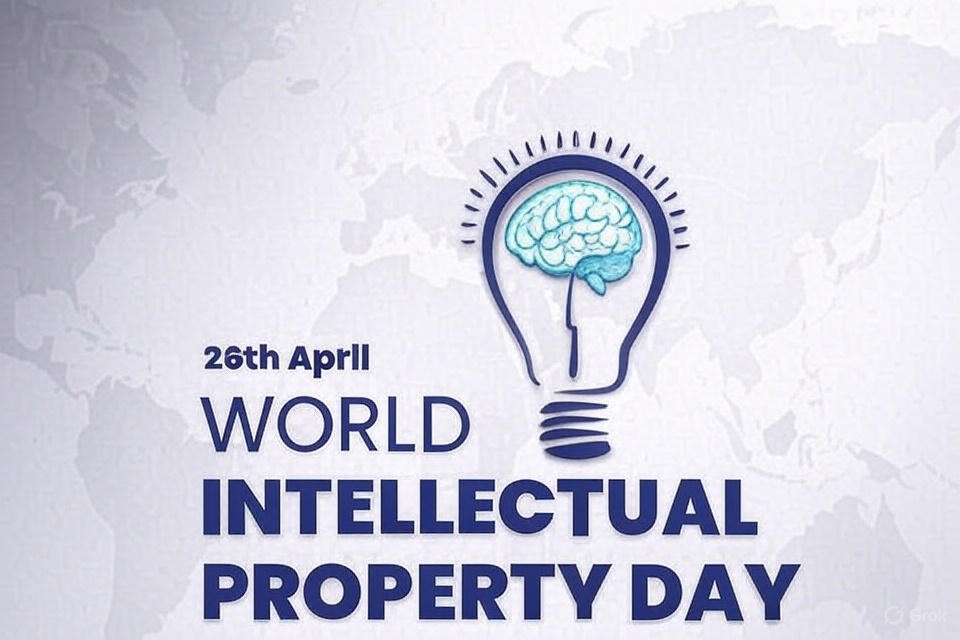भारत, 21 अप्रैल 2025 – भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (National Civil Service Day) मनाया जाता है। यह दिवस देश की सिविल सेवाओं के महत्व को रेखांकित करता है तथा इन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के योगदान को सराहने का अवसर प्रदान करता है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सिविल सेवाएँ भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं, जो शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का इतिहास
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल (भारत के प्रथम गृह मंत्री) ने मेटकाफ हाउस, दिल्ली में आयोजित एक समारोह में नवनियुक्त सिविल सेवकों को संबोधित किया था। इस भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को “भारतीय प्रशासन का स्टील फ्रेम” (Steel Frame of India) कहकर संबोधित किया। उनका यह कथन आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की मजबूती का प्रतीक माना जाता है।
दिवस की स्थापना
सरदार पटेल के इसी ऐतिहासिक संबोधन की याद में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह दिवस सिविल सेवकों के समर्पण, निष्ठा और देश सेवा के प्रति उनके योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है।
भारतीय सिविल सेवाओं का ऐतिहासिक विकास
भारतीय सिविल सेवाओं का इतिहास ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ा हुआ है। आज जिस स्वरूप में हम सिविल सेवाएँ देखते हैं, उसका विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का युग (1854 से पहले)
- सिविल सेवकों का चयन ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा किया जाता था।
- चयनित उम्मीवारों को लंदन के हैलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाता था।
- यह पूरी प्रणाली संरक्षण (पैट्रनज) आधारित थी जिसमें योग्यता से अधिक जान-पहचान महत्वपूर्ण थी।
1854: मैकाले रिपोर्ट और योग्यता आधारित सिविल सेवा की शुरुआत
- लॉर्ड मैकाले की समिति ने 1854 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस रिपोर्ट में योग्यता आधारित सिविल सेवा प्रणाली की सिफारिश की गई।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन की नई प्रणाली शुरू हुई।
- 1855 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई।
प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली की विशेषताएँ
- परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की जाती थी।
- आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष।
- पाठ्यक्रम में यूरोपीय क्लासिक्स को प्रमुखता दी गई थी।
- इन कठिनाइयों के बावजूद 1864 में पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा में सफल हुए।
भारतीयों के लिए संघर्ष (1922 तक)
- भारतीयों ने भारत में भी परीक्षा आयोजित करने की माँग की।
- ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर भारतीयों को रोकने की कोशिश की।
- प्रथम विश्व युद्ध और मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद 1922 में भारत में परीक्षा शुरू हुई।
- इलाहाबाद और दिल्ली में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए।
सार्वजनिक सेवा आयोग का गठन
- भारत सरकार अधिनियम 1919 ने आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
- ली आयोग (1924) ने शीघ्र आयोग स्थापित करने की सिफारिश की।
- 1 अक्टूबर 1926 को भारत में पहली बार सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना।
- सर रॉस बार्कर पहले अध्यक्ष बने।
संवैधानिक परिवर्तन
- 1935 के अधिनियम ने संघीय और प्रांतीय आयोगों का प्रावधान किया।
- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर:
- संघीय सेवा आयोग → संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- अध्यक्ष और सदस्यों का पद संरक्षित रहा।
भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान
भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions) के संगठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यहाँ इन अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:-
- अनुच्छेद 315 : संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग।
- अनुच्छेद 316 : लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान।
- अनुच्छेद 317 : लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाने और अपात्र ठहराने की प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 318 : लोक सेवा आयोगों की सेवा शर्तों और सदस्यों की भर्ती संबंधी नियम बनाने का प्रावधान।
- अनुच्छेद 319 : लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल समाप्ति पर पुनः नियुक्ति या किसी अन्य पद पर नियुक्ति पर रोक।
- अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और कार्यक्षेत्र, जैसे भर्ती प्रक्रियाएँ, पदोन्नति, सेवा नियमों में बदलाव, आदि।
- अनुच्छेद 321 : संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने का प्रावधान।
- अनुच्छेद 322 : संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों के व्यय का व्यय-भार भारतीय संचित कोष (Consolidated Fund) से किया जाएगा।
- अनुच्छेद 323 : लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्टों को राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत करने और उन पर चर्चा करने का प्रावधान।
यह अनुच्छेद भारत में लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिससे वे निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से काम कर सकें।
सिविल सेवाओं का महत्व
भारतीय प्रशासन की रीढ़
सिविल सेवाएँ भारतीय शासन व्यवस्था का मूल आधार हैं। ये सेवाएँ देश की नीति निर्माण, कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
प्रमुख सिविल सेवाएँ
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) – प्रशासनिक प्रबंधन एवं नीति कार्यान्वयन
- भारतीय पुलिस सेवा (IPS) – कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधन
- भारतीय विदेश सेवा (IFS) – अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति
- भारतीय राजस्व सेवा (IRS) – कर प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन
राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का उद्देश्य
- सिविल सेवकों को प्रोत्साहित करना – उनके कठिन परिश्रम एवं समर्पण को सम्मानित करना।
- उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत करना – प्रधानमंत्री पुरस्कार के माध्यम से श्रेष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है।
- सुशासन को बढ़ावा देना – पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- जनता-प्रशासन संवाद को मजबूत करना – आम नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना।
सिविल सेवाओं की चुनौतियाँ
सिविल सेवाएँ देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं:
- भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता की कमी – कुछ मामलों में भ्रष्टाचार प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।
- राजनीतिक दबाव – कई बार सिविल सेवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है।
- संसाधनों की कमी – ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे और फंडिंग की समस्या।
- जनता की बढ़ती उम्मीद – आम नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाएँ कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चुनौती बन जाती हैं।
राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस न केवल सिविल सेवकों के योगदान को सम्मानित करने का दिन है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत, निष्पक्ष और प्रभावी प्रशासन ही देश के विकास की कुंजी है।
सरदार पटेल के शब्दों में – “सिविल सेवक राष्ट्र के वास्तुकार हैं।”
इस अवसर पर हम सभी का कर्तव्य है कि हम सिविल सेवाओं के महत्व को समझें और इनके सुधार के लिए सकारात्मक योगदान दें।
“सेवा, सत्यनिष्ठा और समर्पण” – यही सिविल सेवाओं का मूल मंत्र होना चाहिए।